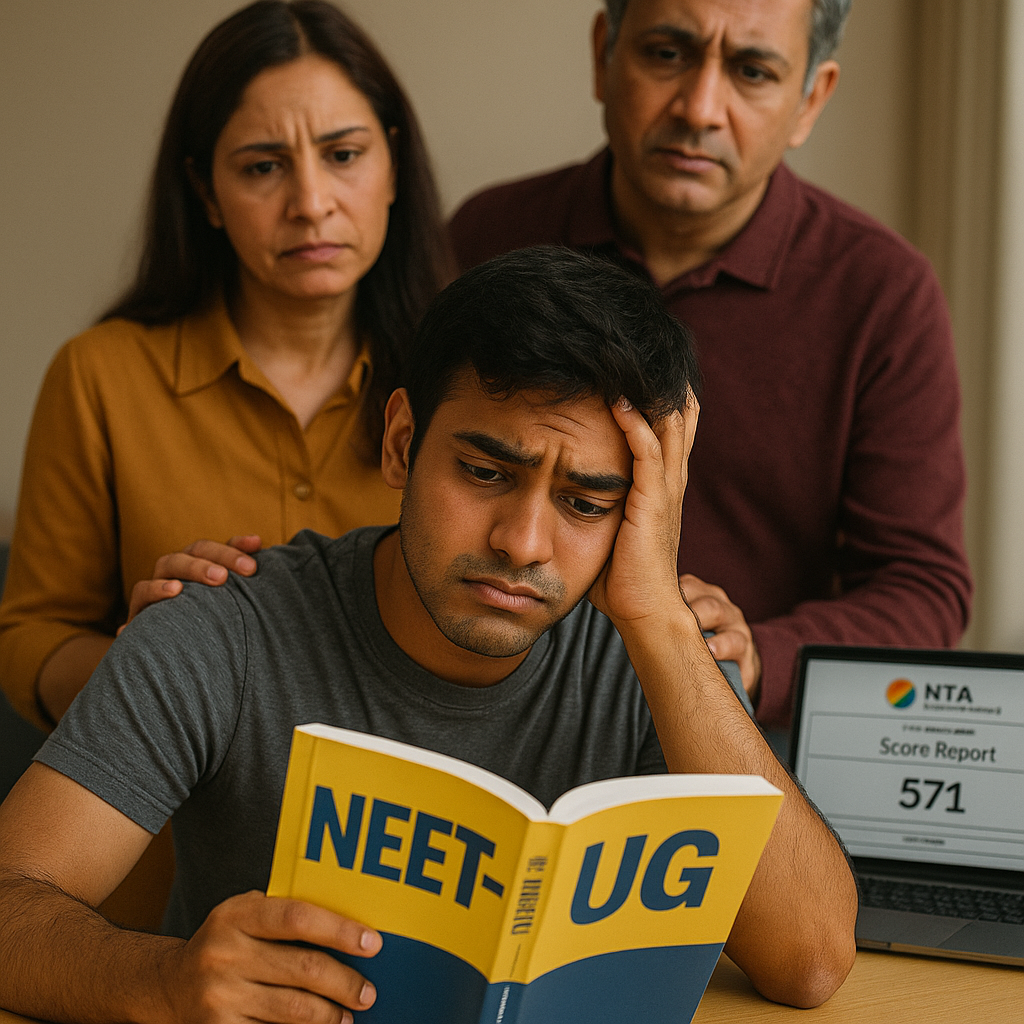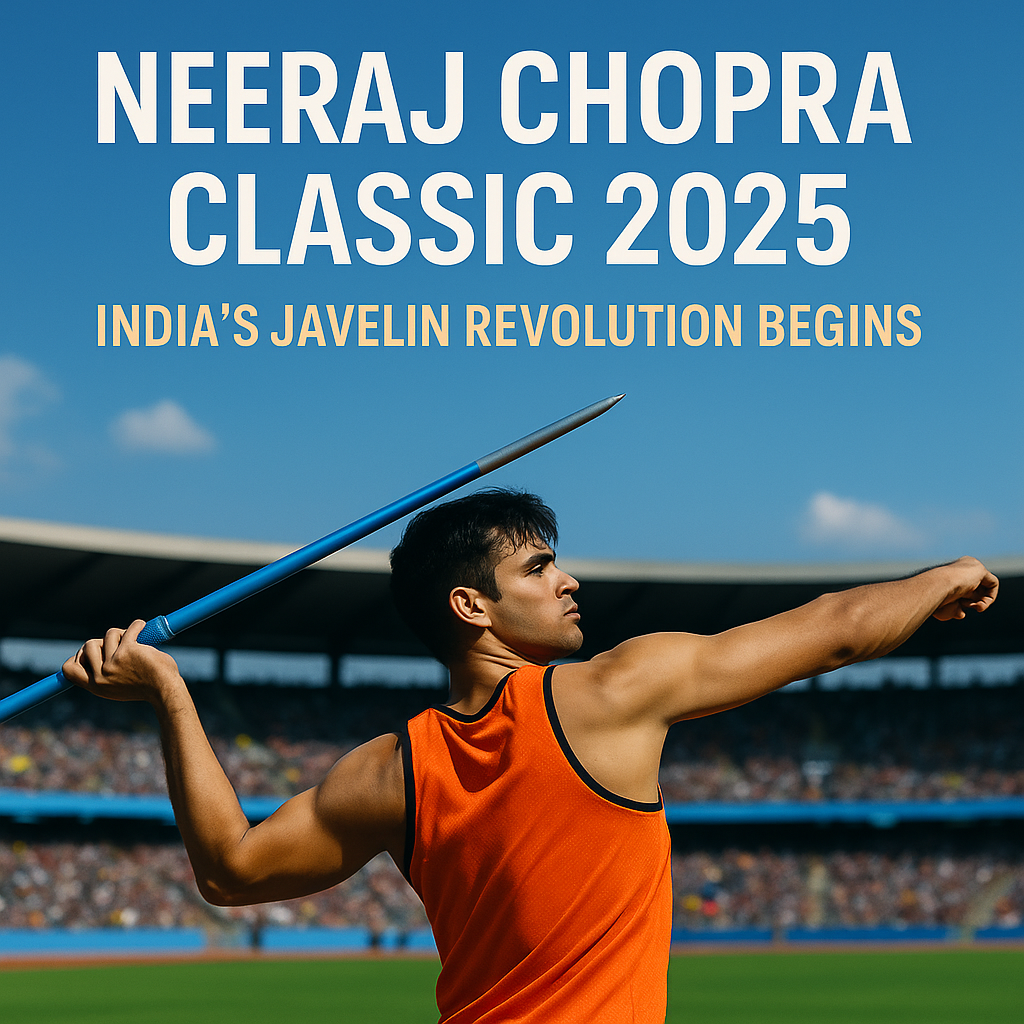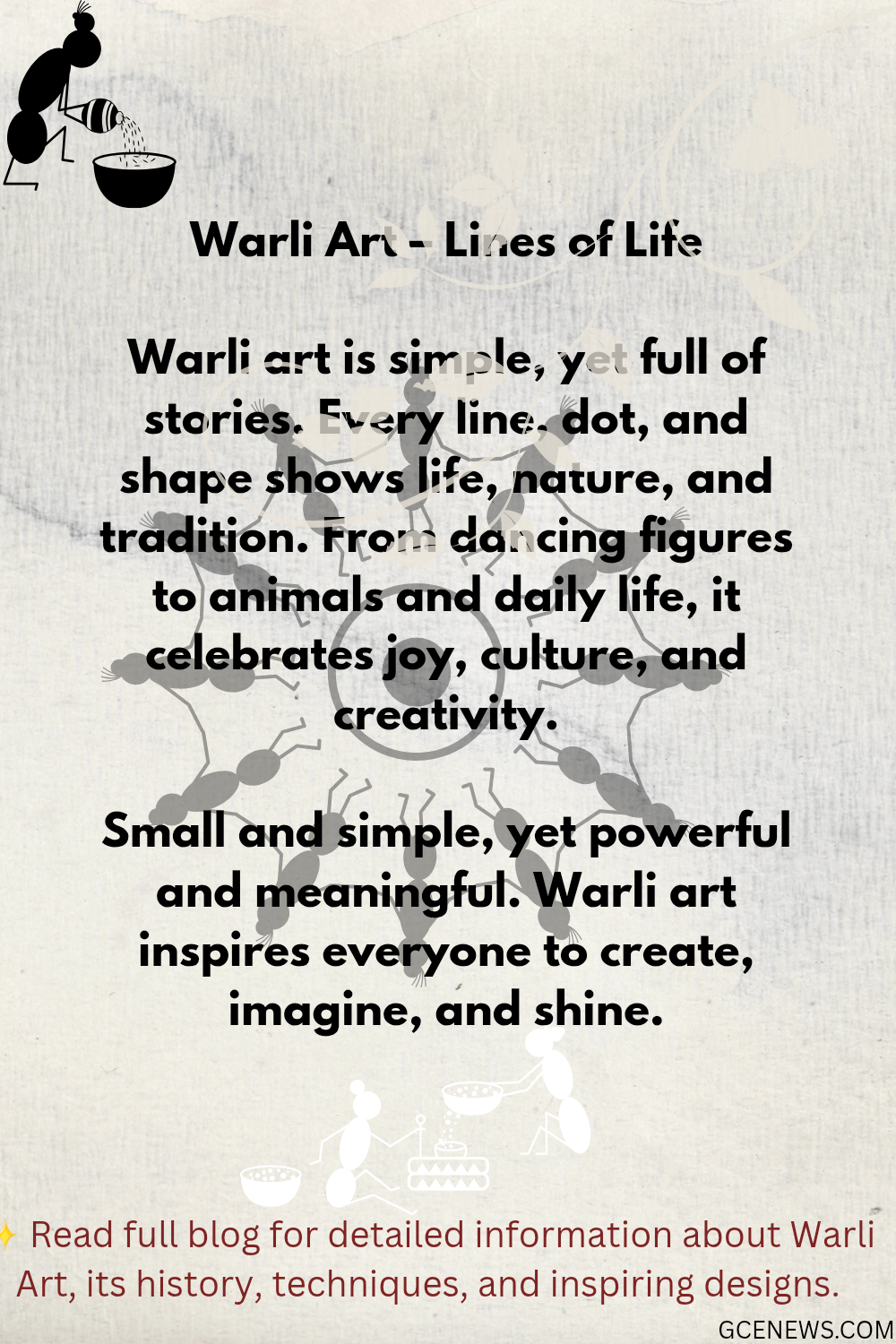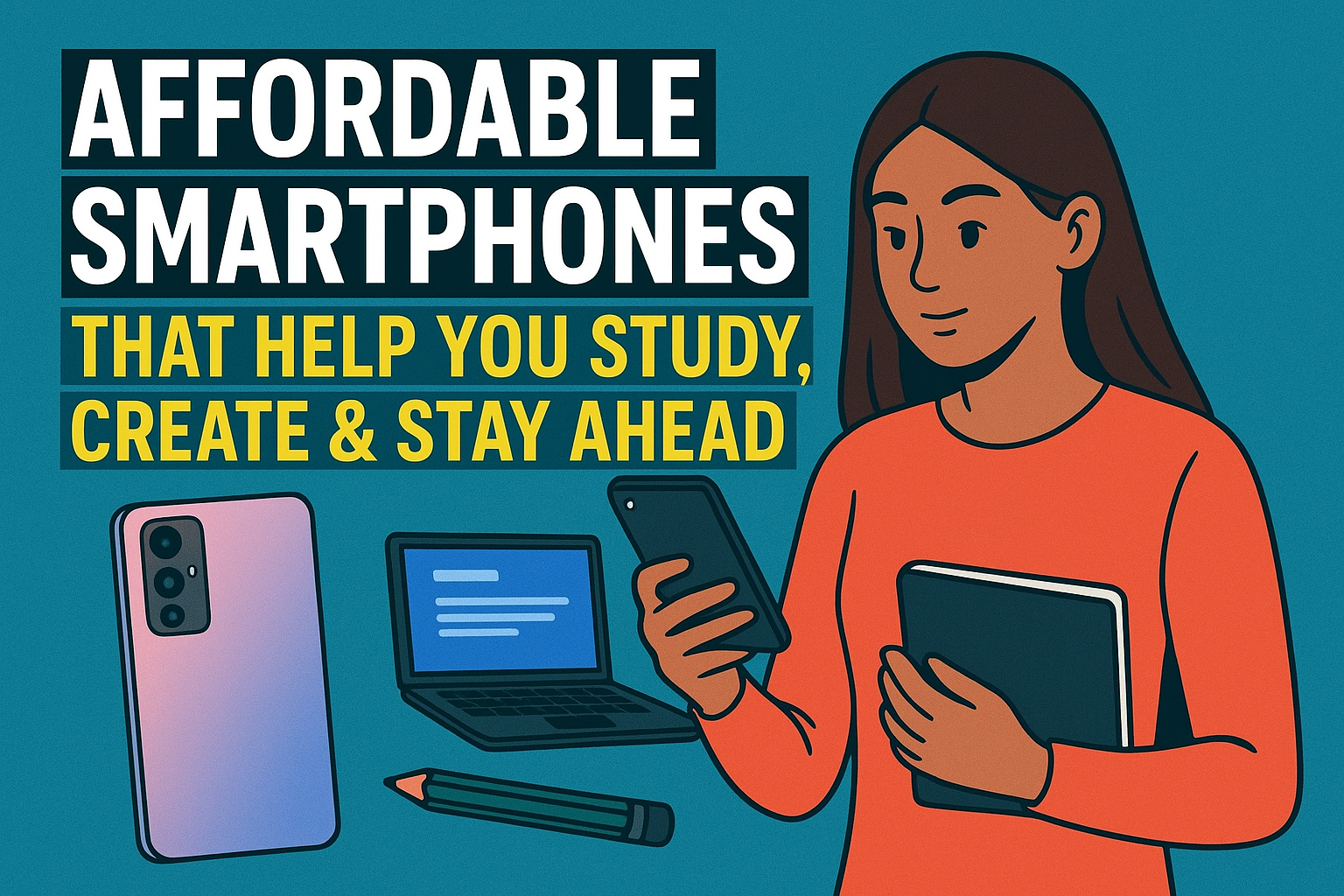ईरान-इज़राइल Conflict एक जटिल Geo-Political संकट

ईरान और इज़रायल के बीच चल रहा युद्ध विश्व मंच पर एक गंभीर और जटिल संकट के रूप में उभरा है। यह संघर्ष न केवल मध्य पूर्व की भू-राजनीति को प्रभावित कर रहा है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी गहरा असर डाल रहा है। भारत, जो मध्य पूर्व के साथ गहरे व्यापारिक और रणनीतिक संबंध रखता है, इस युद्ध के प्रभावों से अछूता नहीं है। इस ब्लॉग में, हम ईरान-इज़रायल युद्ध के ऐतिहासिक संदर्भ, इसके कारण, वर्तमान स्थिति, भारत पर प्रभाव, और संभावित परिणामों पर सामान्य जानकारी के दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे।
ईरान और इज़रायल के बीच तनाव की जड़ें कई दशकों पुरानी हैं। यह संघर्ष धार्मिक, वैचारिक, और भू-राजनीतिक मतभेदों का परिणाम है। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद, जब अयातुल्ला खोमैनी के नेतृत्व में ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई, इज़रायल और ईरान के बीच संबंधों में तनाव बढ़ने लगा। इससे पहले, शाह के शासनकाल में ईरान और इज़रायल के बीच संबंध अपेक्षाकृत मैत्रीपूर्ण थे।
ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा
ईरान का परमाणु कार्यक्रम इस संघर्ष का एक केंद्रीय मुद्दा रहा है। 2015 में, ईरान ने संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी शामिल थे। इस समझौते के तहत, ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का वादा किया था, बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दी गई थी। हालांकि, 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस समझौते से हटने का फैसला किया, जिसके बाद ईरान ने भी धीरे-धीरे अपनी प्रतिबद्धताओं को कम करना शुरू कर दिया।
इज़रायल की चिंताएँ
इज़रायल, जो स्वयं एक परमाणु शक्ति माना जाता है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए एक अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखता है। इज़रायली नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ने बार-बार दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस डर ने इज़रायल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करने के लिए प्रेरित किया है।
प्रॉक्सी युद्ध
ईरान और इज़रायल के बीच प्रत्यक्ष युद्ध से पहले, दोनों देशों ने लेबनान, सीरिया, और यमन जैसे क्षेत्रों में प्रॉक्सी युद्धों के माध्यम से एक-दूसरे के खिलाफ रणनीतिक लड़ाई लड़ी है। ईरान ने हिजबुल्लाह (लेबनान) और हमास (गाजा) जैसे समूहों को समर्थन दिया, जबकि इज़रायल ने सीरिया में ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इज़रायल पर हमले ने इस तनाव को और बढ़ा दिया, जिसके परिणामस्वरूप इज़रायल-हमास युद्ध शुरू हुआ।
वर्तमान युद्ध की शुरुआत
2025 में, ईरान और इज़रायल के बीच तनाव एक पूर्ण युद्ध में बदल गया। इज़रायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों, जैसे नतांज़, फ़ोर्दो, और इस्फ़हान, पर हवाई हमले शुरू किए। इन हमलों में कई शीर्ष ईरानी सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की गई। इज़रायल का दावा है कि ये हमले ईरान की परमाणु क्षमताओं को नष्ट करने के लिए आवश्यक थे।
ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इज़रायल पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिसमें उसने इज़रायली जासूसी एजेंसी मोसाद के एक केंद्र को निशाना बनाने का दावा किया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने इन हमलों को "युद्ध का ऐलान" करार दिया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हस्तक्षेप की मांग की।
अमेरिका की भूमिका
अमेरिका ने इस संघर्ष में इज़रायल का समर्थन किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि अमेरिका ने ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर हमले किए, जिसे उन्होंने "शांति का रास्ता" बताया। हालांकि, ईरान ने दावा किया कि इन हमलों से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि महत्वपूर्ण सामग्री को पहले ही सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था।
वैश्विक प्रतिक्रिया
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और जी-7 देशों ने इस संघर्ष को कम करने का आह्वान किया है, लेकिन कोई ठोस युद्धविराम समझौता नहीं हो सका। इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने इज़रायल की कार्रवाइयों की निंदा की, जबकि जॉर्डन ने स्पष्ट किया कि वह अपने हवाई क्षेत्र को युद्ध के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा।
भारत की स्थिति
भारत ने इस युद्ध में तटस्थ और संतुलित रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर देते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। भारत के लिए यह एक जटिल स्थिति है, क्योंकि वह ईरान और इज़रायल दोनों के साथ मजबूत संबंध रखता है।
ईरान के साथ संबंध
ईरान भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार है। भारत 80% से अधिक कच्चे तेल का आयात फारस की खाड़ी से करता है, और होर्मुज़ जलडमरूमध्य, जो ईरान के नियंत्रण में है, भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, चाबहार बंदरगाह में भारत का निवेश मध्य एशिया तक पहुंच के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
इज़रायल के साथ संबंध
इज़रायल भारत का एक महत्वपूर्ण रक्षा और प्रौद्योगिकी साझेदार है। भारत ने इज़रायल से बराक मिसाइल रक्षा प्रणाली, ड्रोन, और साइबर सुरक्षा तकनीकें खरीदी हैं। दोनों देश आतंकवाद को एक साझा खतरे के रूप में देखते हैं और खुफिया जानकारी साझा करते हैं।
भारत पर प्रभाव
इस युद्ध ने भारत के व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव डाला है। लाल सागर मार्ग, जो भारत के यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, युद्ध के कारण बाधित हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप, शिपिंग लागत और बीमा प्रीमियम बढ़ सकते हैं, जिससे भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होगी।
इसके अलावा, तेल की कीमतों में वृद्धि भारत की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। वाणिज्य मंत्रालय ने इस स्थिति से निपटने के लिए आपात बैठकें बुलाई हैं और वैकल्पिक तेल स्रोतों की तलाश शुरू कर दी है।
भारतीय नागरिकों की सुरक्षा
ईरान में लगभग 4000 भारतीय छात्र और अन्य नागरिक फंसे हुए थे, जिनमें से कई को भारत सरकार ने "ऑपरेशन सिंधु" के तहत सुरक्षित निकाला है। 23 जून 2025 तक, 1713 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। इनमें से अधिकांश लोग बिहार, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और अन्य राज्यों से हैं।
मानवीय संकट
इस युद्ध ने ईरान में एक गंभीर मानवीय संकट पैदा किया है। तेहरान और अन्य शहरों में मिसाइल हमलों और हवाई हमलों के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। ईरानी समाचार एजेंसी फार्स के अनुसार, इज़रायली हमलों में 78 लोग मारे गए और 329 घायल हुए।
नागरिकों का पलायन
तेहरान में लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। कई लोग शहर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों को तेहरान खाली करने की सलाह दी है, और भारत भी अपने नागरिकों को निकालने में जुटा है।
भारतीय छात्रों की स्थिति
ईरान में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र, विशेष रूप से मेडिकल और धार्मिक शिक्षा के लिए गए छात्र, इस युद्ध में फंस गए थे। कई छात्रों ने मिसाइल हमलों और धमाकों की आवाजों का अनुभव किया। भारत सरकार के प्रयासों से, इनमें से कई छात्र सुरक्षित वापस लौट आए हैं, लेकिन कुछ की पढ़ाई बीच में ही छूट गई है।
भविष्य की संभावनाएँ
इस युद्ध का भविष्य अनिश्चित है। यदि यह लंबा चलता है, तो यह विश्व को दो ध्रुवों में बांट सकता है, जैसा कि शीत युद्ध के दौरान देखा गया था। भारत जैसे देश, जो तटस्थता की नीति अपनाते हैं, के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी।
युद्धविराम की संभावना
जी-7 देशों और संयुक्त राष्ट्र ने युद्धविराम की अपील की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। फ्रांस और अन्य यूरोपीय देश ईरान के साथ परमाणु समझौते को पुनर्जनन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इज़रायल और अमेरिका के आक्रामक रुख के कारण यह मुश्किल लग रहा है।
वैश्विक प्रभाव
इस युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तेल की कीमतों में वृद्धि, शिपिंग मार्गों में व्यवधान, और क्षेत्रीय अस्थिरता विश्व व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं। भारत जैसे देशों को अपनी ऊर्जा और व्यापार नीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है।
भारत की भूमिका
भारत, जो ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करता है, इस संकट में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार शांति और बातचीत के महत्व पर जोर दिया है। भारत की यह स्थिति कि "दुनिया को युद्ध की नहीं, बल्कि बुद्ध की जरूरत है," वैश्विक मंच पर उसकी नैतिक स्थिति को मजबूत करती है।
ईरान-इज़रायल युद्ध एक जटिल और बहुआयामी संकट है, जिसके प्रभाव मध्य पूर्व से परे पूरे विश्व में महसूस किए जा रहे हैं। भारत, जो दोनों देशों के साथ महत्वपूर्ण संबंध रखता है, इस युद्ध से आर्थिक और मानवीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। तेल आपूर्ति, व्यापार मार्ग, और नागरिकों की सुरक्षा जैसे मुद्दों ने भारत को सतर्क और सक्रिय रुख अपनाने के लिए मजबूर किया है।
आने वाले समय में, इस युद्ध का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही संभव है। भारत जैसे देश, जो ऐतिहासिक रूप से तटस्थता और शांति की वकालत करते हैं, इस संकट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह युद्ध न केवल मध्य पूर्व, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चेतावनी है कि क्षेत्रीय संघर्षों के वैश्विक परिणाम हो सकते हैं।